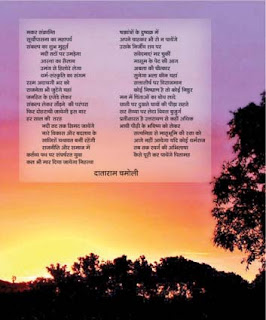Wednesday, May 19, 2010
Monday, April 12, 2010
इस महाकुंभ का संकल्प
 चमोली
चमोलीदेश में प्रयाग (इलाहाबाद), हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में कुंभ मेले आयोजित किये जाते हैं। वर्षों से आयोजित हो रहे इन मेलों पर हर बार लाखों-करोडों रुपये खर्च होते हैं। देश के बडे-बडे नेता, धर्माचार्य, समाजसेवी अपने-अपने ध्वजों, वातानुकूलित् वाहनों तथा हाथी-घोडों की सवारियों के साथ बडी शान से कुंभ में पहुंचते हैं। अपने को एक-दूसरे से बडा समझने के हठ में या पहले स्नान करने की होड में साधु-संतों के बीच खूनी संघर्ष भी हो जाते हैं। नेताओं से लेकर साधु-संतों तक सभी को अपनी छवि चमकाने की लगी रहती है, लेकिन जनहित के मसलों पर सोचने की दिशा में कहीं से भी कोई पहल नहीं होती। यहां तक कि कोई इस दिशा में भी नहीं सोचना चाहता है कि कुंभ के विकास कार्यों के नाम पर कभी गोदावरी, कभी क्षिप्रा तो कभी गंगा में करोडों रुपये बहा दिये जाते हैं। यह बात समझ से परे है कि कुंभ में हर बार विकास कार्य क्यों करवाने पडते हैं। ऐसे स्थायी निर्माण और विकास कार्य क्यों नहीं करवाये जा सकते हैं जिनका जनता को कुंभ की समाप्ति के बाद भी लाभ मिल सके।
सरकारी मशीनरी पर कुंभ मेलों में धन के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहते हैं। जनता चिल्लाती रहती है और नेताओं तथा भ्रष्ट नौकरशाहों का गठजोड सब कुछ सुनते हुए भी बेफिक्र होकर मनमानी करता रहता है। नतीजा यह है कि कुंभ के रूप में वर्षो से चली आ रही संस्कृति का लाभ जनता को नहीं मिल पाता।
इस बार हरिद्वार में सदी का पहला महाकुंभ होने जा रहा है। आगामी कुछ दिनों से स्नान का सिलसिला शुरू हो जायेगा। शासन-प्रशासन बडी मुस्तैदी से मेले की तैयारियों में जुटा हुआ है। यूं समझिये कि तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। राज्य के मुयमंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंक ने प्रमुख सचिव सुभाष कुमार और अपर सचिव निधिमणि त्रिपाठी को खासतौर पर कुंभ पर नजर रखने की जिमेदारी सौंपी है। चारों तरफ कुम्भ मेले की चहल-पहल है। हिमालय की चिंता को लेकर जिस प्रकार नेपाल सरकार के प्रधानमंत्री और मंत्री एवरेस्ट के बेस कैंप में जुटे ठीक उसी तर्ज पर उत्तराखंड सरकार के कर्णधार भी गंगा के किनारे अपनी कैबिनेट बैठक करने की तैयारी में हैं। इसके माध्यम से लोगों को गंगा को स्वच्छ और निर्मल रखने का संदेश दिया जायेगा।
अच्छी बात है कि कुंभ से पहले उत्तराखंड के कर्णधारों को गंगा को स्वच्छ और निर्मल रखने का अहसास हुआ, लेकिन उनका यह प्रयास तभी सार्थक साबित हो सकेगा, जब इसके लिए ठोस धरातल पर काम किया जायेगा। विडंबना ही है कि जो राजनेता और साधु-संत गंगा को बचाने की बडी-बडी बातें कर रहे हैं या करते रहे हैं, वहीं गंगा को प्रदूषित करने में पीछे नहीं हैं। राज्य के एक बडे मंत्री और उनके चेलों पर हरिद्वार में जमीनों पर अवैध कब्ज़ा करने के आरोप लगते रहे हैं। अवैध कब्जों की वजह से कुंभ की धरती सिकुडती जा रही है। साधु-संत भी इसमें पीछे नहीं हैं। हरिद्वार और ऋषिकेश में धर्मशालाओं और आश्रमों का धडल्ले से व्यावसायिक इस्तेमाल हो रहा है। कुछ साधु-संतों के आश्रमों की गंदगी सीधे गंगा में समा रही है। ये वही साधु-संत हैं जो बडे दमखम से गंगा को बचाने का संकल्प लेते हैं।
उत्तराखंड की कैबिनेट बैठक हरिद्वार में हो या फिर हिमालय में यह कैबिनेट और मुख्यमंत्री का अपना फैसला है, इसमें कोई आम आदमी भला क्या कर सकता है, लेकिन इतना अवश्य है कि जनता को गंगा की स्वच्छता का संदेश देने को आतुर कैबिनेट को इस बात का अहसास हो जाना चाहिए कि गंगा आज गौमुख से ही मैली हो चुकी है। गौमुख और बदरीनाथ से ही इसमें तमाम शहरों की गंदगी समा रही है। हाल के वर्षों में हुए शोधों के मुताबिक ऋषिकेश और हरिद्वार में भी इसके पानी में हानिकारक ई कोलीफार्म की काफी मात्रा पायी गयी है। जिस गंगा को बचाने की मुहिम हरिद्वार में शुरू की जाती है, उसकी तमाम धाराएं जल विद्युत परियोजनाओं ने लील ली हैं। ग्लेशियर खतरे में हैं। बडी जल विद्युत परियोजनाओं ने जगह-जगह बडी बेतरतीबी से हिमालय का सीना चीर डाला है। अपने अस्तित्व के लिए जूझता हिमालय आंसू बहा रहा है। वह चिंतित है कि सदियों से उसकी रक्षा करते रहे पहाडवासियों को विशालकाय बांध परियोजनाओं ने अपनी जडों से उजडने के लिए विवश कर दिया है। उनके विकास और आजीविका के लिए कोई ऐसी नीति नहीं बन पा रही है ताकि वे हिमालय में ही ठहरे रहें। पलायन के चलते उनकी बस्तियां वीरान हो चुकी हैं। राज्य के नीति-नियंताओं को यह बात समझ में नहीं आती है कि यदि हिमालय पर बसावट ही नहीं रहेगी तो इसकी रक्षा कौन करेगा? जब हिमालय ही नहीं रहेगा तो फिर गंगा कहां से बचेगी? इसलिए गंगा को बचाने की कोई भी बात वास्तविक धरातल पर ही होनी चाहिए। हवाई नारों और गंगा किनारे कैबिनेट की बैठक कर देने भर से गंगा नहीं बच पायेगी। राज्य के राजनेताओं में जरा भी राजनीतिक इच्छाशक्ति है तो इस महाकुंभ में स्नान कर संकल्प लें कि भविष्य में राज्य में जो भी विकास योजनायें बनेंगी वे हिमालय और गंगा के लिए किसी भी तरह से घातक नहीं होंगी।
Friday, February 12, 2010
हिमालय को बसाये बिना नहीं बचेगी गंगा
- दाताराम चमोली
उत्तराखण्ड हिमालय के 16 हजार गांवों में इस समय करीब 45 हजार गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) हैं। इनमें अधिकांश पर्यावरण संरक्षण और हिमालय को बचाने में जुटे हैं। इसके एवज में उन्हें देश-विदेश से करोड़ों की धन राशि मिल जाती है। लेकिन हालत यह है कि पिछले वर्ष जिन लोगों को उत्तराखण्ड में समाज सेवा के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया, उनके बारे में समाचार माध्यमों से जानकारी पाकर जनता हैरान रह गई। दरअसल जनता उन्हें जानती ही नहीं थी। समाज सेवा के उनके प्रयास उत्तराखण्ड के किस क्षेत्र में रंग लाए, इससे भी लोग अनभिज्ञ हैं। पलायन की पीड़ा और प्राकृतिक संसाधनों के सही नियोजन न होने से एक कहावत प्रचलित हो गयी कि पहाड़ का पानी और जवानी कभी भी वहां के काम नहीं आयी। यह सच भी है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू यह है कि हिमालय बचाने के नाम पर लूट-खसोट करने वालों के लिए वह धरती बेहद उर्वरा साबित हुई है। देश-विदेश से धन बटोरने वाले संगठन यहां कुकुरमुत्तों की तरह पनपते रहे हैं। हिमालय को बचाने के नाम पर हिमालय को बेचा जा रहा है। राज्य की जनता असहाय होकर यह सब देखने को विवश है। सरकारें भी उन्हीें लोगों को तवज्जो देती हंै जो हिमालय या गंगा को बचाने के नाम पर अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति करते हंै या फिर अपनी धार्मिक एवं सामाजिक दुकानें चमका रहे हैं। यही वजह है कि जनता को ऐसे लोगों का कोई समर्थन नहीं मिलता।
दरअसल पहाड़ के लोग भली भांति जानते हैं कि विस्थापन और पलायन अब उनकी नियति बन गई है। परियोजना चाहे तपोवन-विष्णुगाड हो या मनेरी भाली या फिर कोटली भेल, हर जगह नुकसान अंततः उन्हें ही झेलना पड़ेगा। सरकारी नीतियां विकास की आड़ में विनाश को आमंत्रित कर रही हैं। उत्तराखण्ड को ऊर्जा प्रदेश बनाने के लिए पहाड़ों को बुरी तरह खोदा जा रहा है। टिहरीवासियों की तरह ही संपूर्ण पहाड़ के लोगों को उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक जड़ों से काट दिया जाएगा। मध्य हिमालय में 200 से अधिक बांध परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। इनके लिए 700 किलोमीटर लंबी सुरंगों का निर्माण कर धरती को खोखला कर दिया जाएगा। इनके उपर लगभग डेढ़ हजार गांव होंगे। कई गांव बिजली घरों के ऊपर अपने मिटने की घड़ी गिनेंगे। सैकड़ों गांवों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। विष्णुगाड परियोजना के लिए बनी सुरंग के नीचे बने पावर हाउस से संकट में पड़े चांई गांव के लोगों की तरह वे भी अपने भाग्य को कोसेंगे। सरकार नदियों का सीना चीरने पर आमादा है। वह भूल जाती है कि वर्ष 2008 में राज्य की अपनी बिजली की कुल खपत 737 मेगावाट है। अन्य राज्यों को दी जाने वाली बिजली को मिलाकर ऊर्जा की कुल खपत 1500 मेगावाट है। वर्ष 2022 तक राज्य की ऊर्जा की कुल खपत बढ़कर 2849 मेगावाट होगी। इतनी ऊर्जा नदियों के नैसर्गिक प्रवाह को रोके बिना या लघु पन बिजली योजनाओं से भी पैदा की जा सकती है।
विशेषज्ञ शुरू से ही कहते आए हैं कि उत्तराखण्ड हिमालय के लिए बड़ी बांध परियोजनाएं विनाशकारी और लघु जल विद्युत परियोजनाएं हर दृष्टि से वरदान हैं। उत्तराखण्ड राज्य की मांग वास्तव में सत्ता के विकेन्द्रीकरण के साथ ही योजनाओं के विकेन्द्रीकरण को लेकर भी उठी थी। वहां के लोगों को लगता था कि पृथक राज्य गठन के बाद सरकारी विकास योजनाएं पहाड़ की विषम भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखकर बनंेगी, लेकिन आज भी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ही अव्यावहारिक योजनाएं बन रही हैं। बेतरतीब निर्माण कार्यों में विस्फोटकों के बेतहाशा इस्तेमाल से पहाड़ हिल रहे हैं। प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किया जा रहा है। सदियों से जल, जंगल और जमीन की रक्षा करते आ रहे पहाड़वासियों के इन प्राकृतिक संसाधनों से हक-हकूक छीने जाने का सिलसिला जारी है। लोगों को सुखद जीवन जीने की सुविधाएं देने के वजाय पलायन और विस्थापन के लिए मजबूर किया जा रहा है। गंभीर चिंता का विषय है कि पिछले 10 सालों के दौरान उत्तराखण्ड के 10 लाख से ज्यादा लोग स्थाई रूप से अपने गांव-घर छोड़ चुके हैं। करीब दो लाख घरों में ताले पड़ गए हैं। इनमें एक लाख से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों के हैं। युवा शक्ति के बड़ी संख्या में बाहर चले जाने से गांवों में अक्सर यह समस्या खड़ी हो जाती है कि शव को श्मशान तक कैसे पहुंचाया जाए।
असल में गंगा बचाने का सवाल धार्मिक एजेण्डे को मजबूत करने और इसी बहाने किसी के लिए ख्याति अर्जित करने का साधन बना हुआ है। गंगा सिर्फ गंगोत्री से निकलने वाली धारा नहीं है, बल्कि इसकी मुख्य धारा अलकनंदा है। धार्मिक रूप से भी पंच प्रयाग अलकनंदा पर ही हैं। इन पांच नदियों के मिलन से भागीरथी गंगा बनती है। इसलिए इसे सिर्फ 48 किलोमीटर तक शुद्ध रखने की और अविरल बहने देने की बात बहुत कमजोर है। अलकनंदा के उद्गम से लेकर नंदप्रयाग तक इसमें सात बांध प्रस्तावित हैं। इनमें अधिकांश में सुरंगें बननी हैं। कई-कई किलोमीटर तक यह जीवनदायिनी नदी मृत पड़ी है। लेकिन किसी पर्यावरणविद् को इस बात की चिन्ता नहीं है। सही बात यह कि गंगा को बचाने के लिए उन लोगों की भागीदारी जरूरी है जो परंपरागत तरीके से जलधाराओं को बचाने और जल संवर्धन को अपना धर्म समझते हैं। जहां तक पहाड़ का सवाल है वहां सिर्फ गंगा ही गंगा पवित्र नहीं है बल्कि वह सभी 17 नदियां उसकी अराध्य हैं जो उसको जीवन प्रदान करती हैं। उन्हें बचाने के लिए उसका अपना दर्शन है। पेड़ों को बचाने, जमीन को सुरक्षित रखने और पानी के संवर्धन के उसके अपने तरीके ने गंगा और उसकी सहायक नदियों को बचाने की पुरातन से कोशिश की है।
योजनाकारों ने विकास का जो विनाशकारी माॅडल तैयार किया उससे नदियां, जंगल और जमीन उनसे अलग होने लगी। जो नदियां कभी उन्हें भाई-चारे, सौहार्द और सहकारिता का संदेश दिया करती थी अब बांधों ने उनके रोटी-बेटी के रिश्तों तक में दूरियां ला दी हैं। बिगड़ती पारिस्थितिकी और संसाधनों पर से हटते अधिकारों ने जनता को प्रकृति के साथ उसके पौराणिक अन्र्तसंबंधों से दूर किया है। रही-सही कसर सरकारी कानूनों ने पूरी कर दी। वन आधिनियम 1980 जैसेे काले कानून आने के बाद तो जंगल सरकारी हो गये। घास-पत्ती, लकड़ी और पत्थर से छिने हक-हकूकों ने जंगल के दावेदारों को इसके प्रति संवेदनहीन कर दिया। मौजूदा समय में परंपरागत जंगलों के समाप्त होने से चीड़ और यूकेलिप्टस के रोपड़ से यहां के जल स्रोत तेजी के साथ घटे हैं। चैड़ी पत्ती के वृक्षों के अभाव में ग्लोबल वार्मिंग से हिमालय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। ग्लेशियर खिसक रहे हैं। पहाड़ पर नया संकट है। यह भी कहा जा सकता है हिमालय प्रतिकार की मुद्रा में है। कभी पहाड़ के लोग नारा लगाते थे कि ‘हिमालय रूठेगा।’ देश टूटेगा यह अब सत्य साबित हो रहा है। इसी संदर्भ में यह बात महत्वपूर्ण है कि पिछले चार दशक से हिमालय को बचाने के लिए आंदोलनरत जनता की आवाज सुनने के लिए नीति-नियंता तैयार नहीं हैं। लेकिन हवाई नारों और गंगा से कुछ पा लेने के लिए जुटे लोग सरकार के लिए गंगा बचाने के पैरोकार बन बैठे। यही इस आंदोलन और हिमालय को बचाने की त्रासदी है।
पलायन की समस्या ने सीमाओं की सुरक्षा का भी सवाल खड़ा कर दिया है। जब सीमाओं पर लोग ही नहीं रहेंगे, तो उनकी चैकसी कौन करेगा? कभी सरकार इस सीमांत क्षेत्र के लोगों को हथियार चलाने का प्रशिक्षण देती थी। सेवा सुरक्षा बंधुत्व (एसएसबी) के जवान गांव-गांव में जाकर युवाओं, महिलाओं और पुरुषों को दुश्मन से लड़ने के गुर सिखाते थे। यह बात समझ से परे है कि न जाने अब सरकार इसकी जरूरत क्यों महसूस नहीं करती? पलयान और विस्थापन न सिर्फ उत्तराखण्ड बल्कि अन्य हिमालयी राज्यों की भी समस्या है। एक तरह से विकास की गलत होती परिभाषा और संसाधनों से एक साथ ज्यादा लाभ पाने की नफाखोरी की प्रवृत्ति से उपजी स्थितियां हैं। इसका निशाना जल, जंगल और जमीन पर आश्रित सभी समुदायों के लिए खतरे की घंटी है। आदिवासी क्षेत्रों में भी इस नफाखोरी को हिंसक पंजे फैले हैं। हिमालयी राज्यों में 400 से अधिक बांध परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। विशालकाय बांध परियोजनाएं न सिर्फ विस्थापन की समस्या खड़ी करेंगी बल्कि हिमालय में पारिस्थितिकी असंतुलन का कारण भी बनेंगी। इनसे भूस्खलन और भूकंप का खतरा बढ़ेगा और हिमालय का अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। ऐसी स्थिति में न तो गंगा बच पाएगी और न ब्रह्मपुत्र। इंटरनेशनल कमीशन फाॅर स्नो एण्ड आइस के एक अध्ययन के मुताबिक अगले 50 सालों में हिमालय के 50 हिमखंड समाप्त हो जाएंगे। गोमुख ग्लेशियर खतरे में है। 1935 से अब तक इसकी लंबाई 6 किमी और चैड़ाई 2 ़5 किमी घटी है। सन् 2007 में जारी संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार यदि ग्लेशियर इसी तरह सिमटता रहा तो 2030 तक गंगा लुप्त हो जाएगी। ऐसे में गंगा को बचाने के लिए कहीं से भी आवाज उठती है तो वह स्वागत योग्य है। वर्षों सरकारी सेवा का सुख भोगने के बाद रातों-रात कोई पर्यावरणविद् का चोला पहनकर आगे आए या फिर जीवन भर अपने आश्रमों के नजदीक गंगा को मैली होती देखने के बादवजूद 80-90 साल की उम्र में किसी शंकराचार्य को गंगा की रक्षा का बोध हो जाए, इस पर किसी को भला क्या आपत्ति हो सकती है। यह उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है कि वे कब और किस उम्र में गंगा की रक्षा का संकल्प लेते हैं। लेकिन इतना अवश्य है कि गंगा को बचाने की कोई भी बात ठोस धरातल पर ही की जानी चाहिए। गंगा से पहले हिमालय को बचाने की के लिए आवाज उठनी चाहिए। हिमालय बचा रहेगा तो गंगा खुद बच जाएगी। हां, एक अहम बात सच्चाई यह है कि हिमालय को बचाने के लिए उसका बसना बेहद जरूरी है। हिमालय पर आबादी बसी रहनी चाहिए। वहां से लोगों का पलायन देश और दुनिया के हित में नहीं है।
Friday, October 23, 2009
गांव की आछरी
जब हम जवां होंगे, जाने कहां होंगे, बचपन के दिन भी क्या दिन थे. इन पंक्तियों से यही धुन आती है कि पुरानी यादों को सहेजना है, भूलना है, याद रखना है, वगरैह-वगरैह.
हर किसी के जीवन में कुछ किस्से और कहानियां होती हैं. जब हम छोटे होते हैं तो किस तरह हमारे माता-पिता हमें समझाते-बुझाते हैं, हमारे लिए परेशान रहते हैं. ये हमारे बड़े होने पर वो हमें अक्सर याद दिलाया करते हैं कि तूने बचपन में ऐसा किया, वैसा किया आदि- आदि.
जहां तक मेरे बचपन का सवाल है. मैं काफी शरारती था. मां कहती है कि मैंने बचपन में बहुत तंग किया था. मैं बहुत जिद्दी हुआ करता था. किसी बात की जिद कर लेता, तब तक अपनी जिद पर अड़ा रहता था जब तक मेरी मांग पूरी नहीं होती थी.
शायद आप लोगों में कई लोग ऐसे रहे होंगे. आज आप शायद इसे स्वीकारने में झिझक महसूस करें लेकिन यह सच है. कोई भी अपने बचपन की सारी घटनाएं अगर साल-दर-साल कागज पर उकेर दे तो शायद एक उपन्यास बन जाए. लेकिन आप घबराएं नहीं, मैं यहां कोई उपन्यास नहीं लिख रहा हूं. बस आपको एक सत्य घटना बताने जा रहा हूं. आप लोग शायद इस पर विश्वास न करें, लेकिन जो लोग गांवों से जुड़े हुए हैं, खासकर पहाड़ों से उन्हें इस बात का एहसास होगा कि यह सच है.
बात उस समय की है जब मैं छठी सातवीं में पढ़ा करता था. सुबह का स्कूल हुआ करता था. सुबह सात बजे से दोपहर 12-1 बजे तक. स्कूल से लौटने के बाद हम लोग जब घर आते थे तो खाना खाने के बाद पशुओं को चराने के लिए जंगलों में जाया करते थे और सूरज ढलते ही घरों की ओर लौट आते थे.
जंगल जाने से पहले मां-बाप ढेर सारे उपदेश देते थे. जैसे बेटा जंगल में कहीं इधर-उधर भटक मत जाना. सोना नहीं, कहीं पता चला कि तुम सो गए और पशु किसी के खेत में चले गए और लोग उन्हें सिंगुड़ी ले जाएं. (सिंगुड़ी उसे कहते हैं जब पशु किसी का नुकसान करते हैं, तो जिसका नुकसान हुआ हो वह पशुओं को अपने घर ले जाता है और आर्थिक दंड देने के बाद ही उन्हें अपने कब्जे से मुक्त करता है.)
बेटा सोना मत, कहीं आछरी, मातरी ले गई तो जान से ही हाथ धोना पड़ेगा. (आछरी या मातरी उसे कहते हैं जिसे शहरी भाषा में परी कहा जाता है.)
रोजाना की तरह ही एक दिन हम लोग जंगल में गए थे. उस दिन गांव की ही एक लड़की हमारे साथ जंगल में पशुओं को चुंगाने आई थी. शायद वह इससे भी पहले जंगल गई हो, लेकिन मेरे साथ उस दिन पहली बार आई थी. उस दिन हम लोग रोज की तरह ही खेल रहे थे कि खेल ही खेल में वह जोर जोर से चीखने-चिल्लाने लगी.
हम लोगों को लगा जैसे ऐसे ही चिल्ला रही है. लेकिन चुप कराने पर भी जब वह चुप नहीं हुई तो सब लोग घबरा गए कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया जो जो चीखने-चिल्लाने लगी.
डर के मारे सबकी हालत पतली हो रही थी. इसी बीच एक घटना अचानक और घट गई वह घर आने के बजाय जंगल की ओर जाने लगी. अब किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए. सबने थोड़ी-थोड़ी हिम्मत जुटाई और उसे पकड़ने लगे, जैसे ही उसके करीब गए तो उसने अपनी आंखें घुमाई और बाल बिखरा दिए. हूं... आओ देखती हूं कौन मुझे रोकता है.
वह फिर दहाड़ी. हूं.... हूस्स उसको चेहरा देखने लायक था.
अब सबकी हवा निकल गई. कि आखिर करें तो क्या करें. वह आगे बढ़ती ही जा रही थी और हम लोग उसके पीछे-पीछे जा रहे थे. लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसे पकड़ ले.
एक बार हम सबने हिम्मत जुटाई और उसे घसीटते हुए थोड़ा नीचे ले आए. बस हमारा इतना ही करना था कि वह और भी आग बबूला हो गई.
जोर- जोर से चीखने लगी, हूं... हूं... हूं.... shhhhh. किसी को नहीं छोडूंगी, सब के सब मारे जाओगे. आज देखती हूं तुम्हें कौन बचाता है. फिर वही हूं... हूं... हूं.... shhhhh.
इस बीच अचानक न जाने मुझे क्या हुआ. मैं जोर से चिल्लाया. और मैंने उसके बाल खींचें और एक-दो जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिए. उसके बाद से अचानक एकदम स्थिति ठीक हो गई.
वह सामान्य हो गई और हम सब लोग घर की ओर चल पड़े.
घर आने जब पूरी बात मां को बताई, तो मां ने भगवान का लाख-लाख शुक्रिया अदा किया.
हे भगवान तूने मेरे बच्चे को सही सलामत घर पहुंचा दिया. हे कुल देवता ये सब तेरी कृपा है जो मेरे बच्चे सही सलामत घर लौट आए, ना जाने वो हरामजादी क्या-क्या करती मेरे बच्चों के साथ.
मैंने मां से पूछा तो मां ने बताया कि वह मातरी थी और तुम्हें अपने वश में करके वह पहाड़ पर ले जाती और वहां निचे गिरा देती या तुम लोगों के साथ कुछ भी कर सकती थी.
अब मैं और भी डर गया.मैंने पूछा, मां लेकिन मैं भी तो चिल्लाया था और उसको एक-दो थप्पड़ मारे थे.
मां बोली, वह हमारे कुल देवता तेरी सहायता के लिए आए थे. ये सब उनकी कृपा थी. इतने में मेरी आंखों से आंसू टपक पड़े.
शायद मां समझ गई कि मैं डर गया हूं.
मां बोली, चल कुछ खा ले तुझे भूख लगी होगी.
मैंने कहा, मां लेकिन...मां बोली, लेकिन-वेकिन कुछ नहीं पहले कुछ खा ले फिर...मां, फिर... कुछ नहीं बोली न कुछ नहीं.... कुछ खा ले और मैं खाने के लिए रसाईघर में चल दिया.
उसके बाद मैंने खाना खाया और सब सामान्य हो गया.
तीन दिन बाद फिर पता लगा कि गांव में किसी महिला की तबियत अचान खराब हो गई. सुना कि वह खेत से घर लौट रही थी और घर पर आते ही लुंज-मुंज (अचेत अवस्था में) हो गई.
गांव के सारे लोग इकट्ठा हो गए. देवता को बुलाया गया. देवता का धामी आया और झूलने लगा, उसने बताया कि यह तो तीन दिन पहले ही गांव में प्रवेश कर गई है. इसे गांव से भगाया जाए. सबने देवता से आग्रह किया कि आप ही कुछ करें.
देवता ने चावल फेंके और कुछ देर बाद वह महिला ठीक हो गई. इतने में मैं भी पहुंच गया. जैसे कि गांव में अक्सर होता है कि किसी के घर में यदि कुछ हो जाए तो सारे लोग एकट्ठे हो जाते हैं. मैं पहुंचा तो गांव के ही एक बुजुर्ग आदमी से मैंने पूछा, चाचा क्या हुआ?
फिर उन्होंने विस्तार से बताया-
यह लड़की फलां गांव की है, यह जवान लड़की थी और अल्पायु में मर गई, इसके घर वालों ने इसका क्रियाकर्म किया या नहीं, भगवान जाने. अब यह सबको परेशान कर रही है.
अब यह दर-दर भटक रही है और लोगों को परेशान कर रही है. मैंने कहा, चाचा लेकिन, ऐसा क्यों?
इस पर चाचा हसंते हुए बोले, बेटा अभी तुम छोटे हो, जब बड़े हो जाओगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा ये सब क्या होता है.
जारी...
रावत शशि मोहन पहाड़ी
Tuesday, October 6, 2009
काँच की बरनी और दो कप चाय - एक बोध कथा
यह बोध कथा मेरे मित्र महेंद्र सिंह बोरा ने मुझे मेल की। मुझे लगा की इसे अपने और मित्रों तक भी पहुँचाया जाय। इसीलिए ब्लॉग पर पोस्ट कर रहा हूँ।